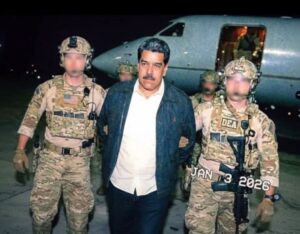कागजी न रह जाए कुनमिंग-माॅन्ट्रियाल फ्रेमवर्क
1 min read

याद होगा कि गत वर्ष कनाडा के माॅन्ट्रियाल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (सीओपी 15) में सदस्य देशों ने जैव प्रजातियों के तेज और स्थिर नुकसान को रोकने के लिए एक नए ढांचे पर सहमति जतायी थी। यह सम्मेलन इस मायने में महत्वपूर्ण था कि भारत समेत सभी 196 देशों ने पास्थितिकी तंत्र को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए एक नए लक्ष्य की जरुरत पर बल दिया था।
इसे ध्यान में रखते हुए ही इस सम्मेलन में कुनमिंग-माॅन्ट्रियाल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाने की बात कही गयी जो कि 2050 के लिए 4 और 2030 के लिए 23 लक्ष्यों को निर्धारित करता है। 2030 के इन लक्ष्यों में निम्नीकृत क्षेत्रों के लिए सुरक्षा, जैव संरक्षण के लिए संसाधनों की उपलब्धता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और समुद्र के अम्लीकरण को कम करना, आक्रामक विदेशी प्रजातियों कें प्रसार को कम करना और जैव विविधता समर्थक विविधयों को अपनाना इत्यादि प्रमुख है।
इसी तरह 2050 के लिए जिन चार लक्ष्यों को निर्धारित किया गया उनमें विलुप्त होने वाले पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ जैव विविधता द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को मापना व मूल्यांकन करना इत्यादि पर जोर दिया गया। भारत ने इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया था कि विकासशील देशों को जैवविविधता को हुए नुकसान को रोकने के लिए 2020 के बाद की वैश्विक रुपरेखा को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक नया समर्पित कोष बनाया जाए। भारत ने तर्क रखा कि जैव विविधता का संरक्षण साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं पर आधारित होना चाहिए।
इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने वर्ष 2030 तक पृथ्वी के 30 फीसदी हिस्से को प्रकृति के लिए संरक्षित करने की हामी के साथ दुनिया भर में दी जा रही उन सब्सिडी में सालाना 500 अरब डाॅलर कमी लाने पर भी सहमति जतायी जो पर्यावरण के लिहाज से बेहद नुकसानदेह है। ध्यान दें तो मौजूदा समय में सिर्फ 17 फीसद हिस्सा ही प्रकृति के लिए संरक्षित है। ऐसे में सात वर्षों के दरम्यान 30 फीसद हिस्सा प्रकृति के लिए संरक्षित करना बड़ी चुनौती है।
इस चुनौती को साधने के लिए सभी देशों को अपनी-अपनी नीतियों और विकास संबंधी परियोजनाओं में आमुलचूल परिवर्तन लाने होंगे जो कि ऐसा होता नहीं दिख रहा है। विकसित देशों के लिए तो यह आसान है लेकिन विकासशील देशों को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई समस्याओं से जूझना होगा। मसलन उन्हें अपनी प्रकृति आधारित विकास परियोजनाओं पर ब्रेक लगाना होगा। इसके लिए वे फंड की डिमांड की बात करते हैं।
सवाल लाजिमी है कि यह फंड कहां से आएगा। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता वित्तीय कोष के तहत कुछ रकम इकठ्ठा किया जा सकता है। लेकिन यह रकम ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगा। विकासशील और गरीब देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण की है। एक अरसे से सभी देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण का संकल्प व्यक्त किया जाता रहा है। लेकिन सच्चाई है कि इस मसले पर कभी भी गंभीरता नहीं दिखायी गयी।
दरअसल विकास को लेकर सभी देशों की अपनी-अपनी प्राथमिकताएं और अपेक्षाएं हैं। नतीजा सामने है। अभी गत वर्ष ही वल्र्ड वाइल्ड फंड एवं लंदन की जूओलाॅजिकल सोसायटी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि दुनिया भर में हो रही जंगलों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले चार दशकों में वन्य जीवों की संख्या में भारी कमी आयी है। इस रिपोर्ट में 1970 से 2012 तक वन्य जीवों की संख्या में 58 प्रतिशत की कमी बतायी गयी।
एक अन्य आंकड़े के मुताबिक भीड़ बकरियों जैसे जानवरों के उपचार में दिए जा रहे खतरनाक दवाओं के कारण भी पिछले 20 सालों में दक्षिण-पूर्व एशिया में गिद्धों की संख्या में कमी आयी है। भारत में पिछले एक दशक में गिद्धों की संख्या में 97 प्रतिशत की कमी आयी है। गिद्धों की तरह अन्य प्रजातियां भी तेजी से विलुप्त हो रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 12000 वर्ष पहले हिमयुग के खत्म होने के बाद होलोसीन युग शुरु हुआ था। इस युग में धरती पर मानव सभ्यता ने जन्म लिया।
इसमें मौसम चक्र स्थिर था इसलिए स्थलीय और जलीय जीव पनप सके। लेकिन बीसवीं सदी के मध्य से जिस तरह परमाणु उर्जा के प्रयोग का दौर शुरु हुआ है और बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हो रही है, उससे होलोसीन युग की समाप्ति का अंदेशा बढ़ गया है। उसी का असर है कि आज वन्य जीवों को अस्तित्व के संकट से गुजरना पड़ रहा है। वन्य जीवों के वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो पृथ्वी के समस्त जीवधारियों में से ज्ञात एवं वर्णित जातियों की संख्या लगभग 18 लाख है।
लेकिन यह संख्या वास्तविक संख्या के तकरीबन 15 फीसद से कम है। जहां तक भारत का सवाल है तो यहां विभिन्न प्रकार के जीव बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जीवों की लगभग 75 हजार प्रजातियां पायी जाती है। भारत में जीवों के संरक्षण के लिए कई कानून बने हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जीवों का संहार जारी है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले सैकड़ों सालों में मनुष्य जाति ने विकास के नाम पर करोड़ों हेक्टेयर वनों विनाश किया है जिससे एक तिहाई से अधिक प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं।
इसी तरह जीवों की संख्या में भी 50 फीसद की कमी आयी है। गौर करें तो वन्य जीवन पर खतरे के महत्वूर्ण कारणों में 71.8 प्रतिशत शिकार, 34.7 प्रतिशत बढ़ता शहरीकरण, 19.4 प्रतिशत ग्लोबल वार्मिंग, 21.9 प्रतिशत प्रदूषण और 62.2 प्रतिशत खेत बनते जंगल मुख्य रुप से जिम्मेदार हैं। अभी गत वर्ष ही नेशनल आॅटोनाॅमस यूनिवर्सिटी आॅफ मैक्सिको और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि आगामी वर्षों में जीवों की कुल प्रजातियों में से 75 प्रतिशत विलुप्त हो सकती हैं।
शोध के नतीजे बताते हैं कि अब तक पृथ्वी पर जितने जीव हुए उनमें से 50 प्रतिशत से अधिक लुप्त हो चुके हैं। इनकी संख्या अरबों में है। ऐसे में उचित होगा कि दुनिया के सभी देश कुनमिंग-माॅन्ट्रियाल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को मूर्त रुप देने के लिए ठोस पहल करें।
अरविंद जयतिलक (लेखक/स्तंभकार)