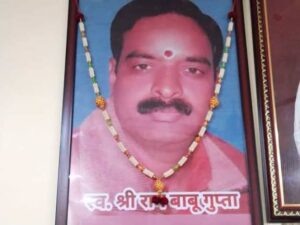Natural Disaster : बाढ़ और भूस्खलन: प्रकृति की चेतावनी या इंसानी लापरवाही ?
1 min read

विशेष रिपोर्ट – रवि नाथ दीक्षित
भारत इस समय दो परस्पर विरोधी जल संकटों का सामना कर रहा है। एक ओर कई राज्य पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, तो दूसरी ओर बरसात के मौसम में बाढ़ और भूस्खलन का तांडव जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर देता है। हर साल मानसून आते ही हजारों लोग विस्थापित हो जाते हैं, लाखों हेक्टेयर फसलें नष्ट हो जाती हैं और करोड़ों की संपत्ति बह जाती है।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सब केवल प्रकृति की मर्जी है या फिर हमारी नीतिगत चूक और लापरवाह विकास भी इसका मुख्य कारण हैं? सच्चाई यह है कि प्राकृतिक आपदाओं के पीछे मानवीय गतिविधियाँ और पर्यावरण से छेड़छाड़ बड़ी भूमिका निभा रही हैं।
क्यों बढ़ रहा है संकट?
बीते कुछ दशकों में हमने जिस तरह अनियोजित शहरीकरण, अवैध खनन और जंगलों की कटाई को बढ़ावा दिया है, उसका असर अब साफ़ दिखने लगा है। पहले गाँवों के तालाब और पोखर वर्षा जल को सोख लेते थे।नदियाँ स्वाभाविक रूप से अपनी गहराई बनाए रखती थीं। पहाड़ों पर हरियाली ढलानों को थामे रहती थी।
लेकिन अब हालात उलट गए हैं। शहरों में जलनिकासी की प्राकृतिक व्यवस्था खत्म हो गई है। गाँवों में नालों और तालाबों पर कब्ज़ा हो चुका है। नदियों से रेत और गाद की निकासी बंद है। और पहाड़ों पर अंधाधुंध कटाई ने मिट्टी को कमजोर बना दिया है।
न्यायपालिका का चेतावनी भरा संदेश
देश की सर्वोच्च अदालत ने कई बार टिप्पणी की है कि इंसान ने प्रकृति से छेड़छाड़ की है और अब वही प्रकृति पलटवार कर रही है। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि सरकारें और समाज समय रहते नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियाँ और भी बड़े संकट का सामना करेंगी। यह स्पष्ट संकेत है कि पर्यावरणीय संतुलन बहाल किए बिना सुरक्षित भविष्य की कल्पना असंभव है।
उत्तर प्रदेश: तराई में हर साल की तबाही
उत्तर प्रदेश का तराई इलाका बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित रहता है। गंगा, यमुना, घाघरा, राप्ती और सरयू जैसी नदियाँ यहाँ बहती हैं।
गंगा: लंबाई लगभग 1300 किमी
यमुना: करीब 1320 किमी
घाघरा: लगभग 600 किमी
बहराइच, लखीमपुर, बलरामपुर, बाराबंकी और सीतापुर जैसे जिलों में हर वर्ष बाढ़ कहर बरपाती है। मुख्य कारण है नदियों की उथली होती धारा।राप्ती: दो दशक पहले इसकी डिस्चार्ज क्षमता 3–5 मीटर थी, जो अब घटकर केवल 200–350 सेंटीमीटर रह गई। सरयू: गाद की सफाई कभी नहीं हुई। ऊपर से अवैध खनन ने स्थिति और बिगाड़ दी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नियमित गाद निकासी होती तो इन जिलों को हर साल बाढ़ से इतनी तबाही न झेलनी पड़ती।
हिमाचल प्रदेश: पहाड़ों का कमजोर होता ढांचा
हिमाचल प्रदेश में इस बार भी भारी बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को तहस-नहस कर दिया। यहाँ की त्रासदी केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि मानवीय लालच से भी जुड़ी है।
मुख्य कारण:
1-पहाड़ों की अंधाधुंध कटिंग 2-नदियों का अवैध खनन 3- जंगलों का अवैध कटान
पेड़ मिट्टी को थामने का काम करते हैं। लेकिन जब हरियाली उजड़ती है तो ढलान कमजोर हो जाते हैं और बारिश के साथ भूस्खलन की घटनाएँ आम हो जाती हैं।
अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच उद्योग विभाग ने अवैध खनन के 895 मामले दर्ज किए और 44.31 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कई वाहन और मशीनें जब्त की गईं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि अवैध खनन और पेड़ों की कटाई सीधे तौर पर आपदाओं का कारण हैं।
दिल्ली: यमुना की आधी हो चुकी क्षमता
दिल्ली की जीवनरेखा मानी जाने वाली यमुना नदी की हालत बेहद खराब हो चुकी है।
1978: हथिनी कुंड से 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो जलस्तर 207.49 मीटर दर्ज हुआ।
2023: केवल 3.59 क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर भी जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुँच गया।
2025: 3.29 क्यूसेक पानी पर स्तर 204.88 मीटर रहा।
इसका मतलब है कि पिछले 40 सालों में यमुना की जलधारण क्षमता आधी हो गई है। यदि समय-समय पर इसकी सफाई और गाद हटाने का काम होता तो राजधानी को यह संकट नहीं झेलना पड़ता।
पंजाब: नदियों पर अवैध खनन का साया
पंजाब में सतलुज, ब्यास और रावी नदियाँ अक्सर बाढ़ का कारण बनती हैं।
सतलुज: मैदान में उतरने पर इसकी क्षमता 2.30 लाख क्यूसेक रहती है। हरिके हैडवर्क्स पर ब्यास मिलने से यह 3.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ जाती है।
ब्यास: ‘कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट’ क्षेत्र घोषित होने के कारण यहाँ खनन पर पाबंदी है। राज्य और केंद्र के बीच टकराव ने स्थिति को और बिगाड़ा।
रावी: यह नदी भारत-पाक सीमा से गुजरती है। कानूनी खनन यहाँ वर्जित है, लेकिन अवैध खनन बड़े पैमाने पर जारी है। सेना भी इसे सुरक्षा के लिए खतरा बता चुकी है।
जम्मू-कश्मीर: विकास कार्यों का दुष्परिणाम
जम्मू-कश्मीर में सड़कों, रेलवे और सुरंग परियोजनाओं के लिए पहाड़ों को बड़े पैमाने पर काटा गया। इससे ढलानों की मजबूती कम हो गई और बारिश की पहली तेज बौछार में ही भूस्खलन की घटनाएँ सामने आने लगीं।
पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि निर्माण कार्यों में मानकों का पालन किया जाता तो यह नुकसान इतना भयावह नहीं होता।
विशेषज्ञों की राय और समाधान
पर्यावरणविद मानते हैं कि बाढ़ और भूस्खलन को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनके असर को कम करना संभव है।
1. गाद निकासी: नदियों की गहराई बढ़ाकर जल संग्रहण क्षमता दोगुनी की जा सकती है।
2. खनन पर नियंत्रण: नदियों से अवैध रेत-बालू निकालना रोकना अनिवार्य है।
3. हरित आवरण की रक्षा: जंगलों की कटाई पर रोक लगाकर वनीकरण को बढ़ावा देना होगा।
4. अतिक्रमण हटाना: तालाबों और नालों पर से कब्ज़ा हटाकर प्राकृतिक जलधाराओं को मुक्त करना जरूरी है।
5. आपदा प्रबंधन: प्रभावित जिलों में आधुनिक चेतावनी प्रणाली और स्थायी राहत केंद्र विकसित करने होंगे।
जल व आपदा प्रबंधन पर सरकार की जिम्मेदारी
हर बार आपदा के समय केंद्र और राज्य सरकारें राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय हो जाती हैं। लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कदम बहुत धीमी गति से उठाए जाते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि एक राष्ट्रीय नदी प्रबंधन नीति बनाई जाए जिसमें गाद निकासी, खनन नियंत्रण और हरित आवरण की सुरक्षा को प्राथमिकता मिले, तो बाढ़ और भूस्खलन की मार काफी हद तक कम हो सकती है।
बाढ़ और भूस्खलन केवल मौसम की मार नहीं हैं। यह हमारी लापरवाह नीतियों, अव्यवस्थित विकास और प्रकृति से छेड़छाड़ का परिणाम भी हैं। जब तक हम विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन नहीं साधेंगे, हर बरसात विनाश का संदेश लेकर आएगी।
अब समय है कि हम चेतें। ठोस नीतियाँ बनें, उनका सख्ती से पालन हो और आम जनता भी जागरूक बने। तभी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित वातावरण दिया जा सकता है।